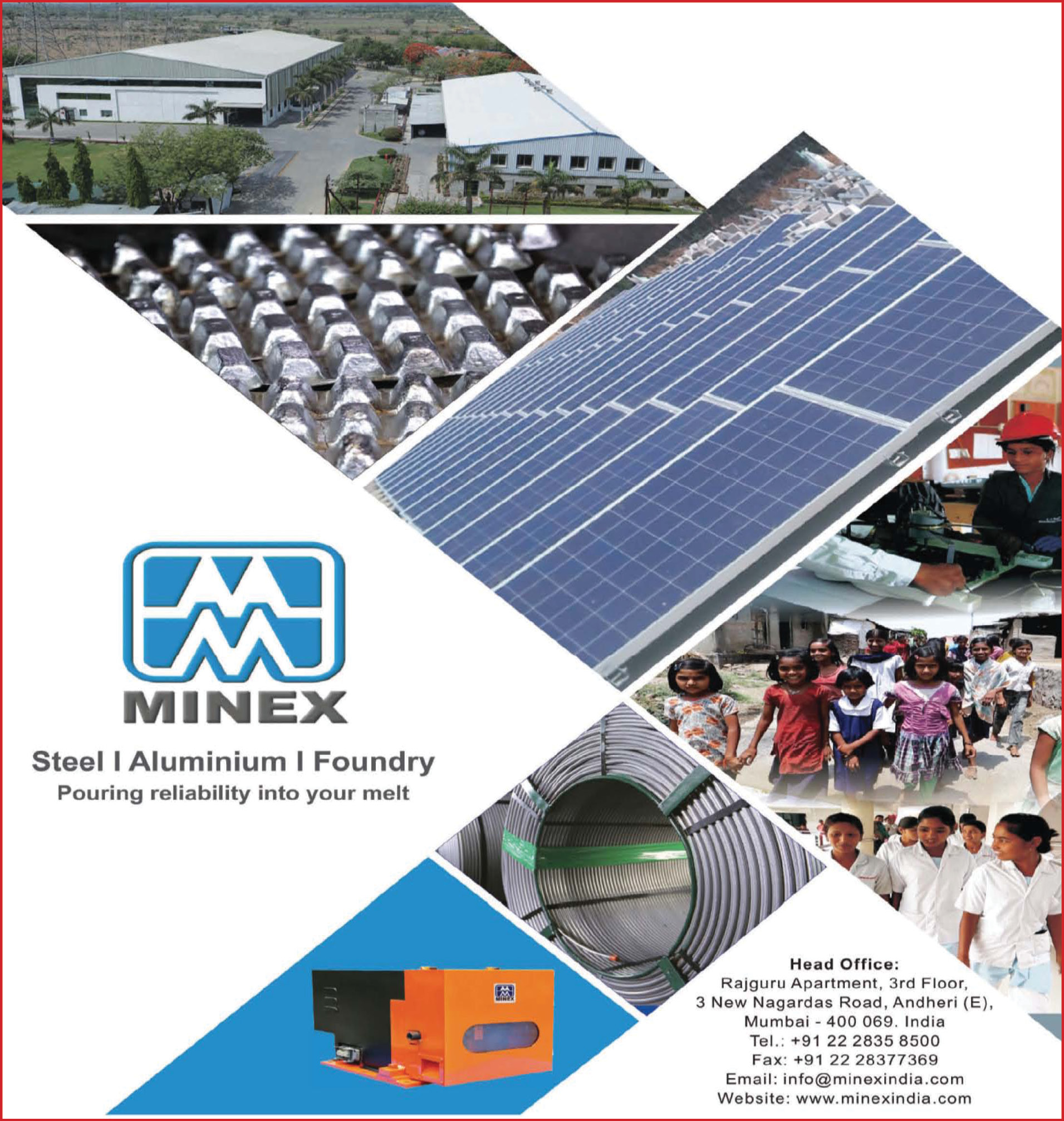आपातकाल के 50 साल: आखिर कहां पहुंची संवैधानिक और राजनीतिक यात्रा

भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में दो अहम पड़ाव हैं: 75 साल की लोकतांत्रिक सफलता और 50 साल पहले लगा आपातकाल।आपातकाल से पहले, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने पुत्र संजय गांधी और चाटुकारों पर अत्यधिक निर्भर हो चुकी थीं, जिससे सत्ता निरंकुश होने लगी थी।पी.एन. धर जैसे तत्कालीन अधिकारियों ने भी इसे ‘गैर-संवैधानिक गतिविधियों का केंद्र’ बताया।
भारत में आजादी के बाद राजनीतिक तौर पर दो महत्वपूर्ण पड़ाव दृष्टिगोचर होते हैं। एक जब देश ने अपने लोकतांत्रिक यात्रा के पचहतर साल पूरा किया। दूसरा जब आज से पचास साल पहले लोकतंत्र में प्राप्त नागरिक अधिकारों पर पाबंदी लगाते हुए देश में आपातकाल लागू किया गया। आपातकाल लागू होने के कुछ पहले से ही प्रधामनंत्री इन्दिरा गांधी अपने चाटुकार मण्डली और अपने पुत्र संजय गांधी पर बहुत हद निर्भर हो चुकी थी।
खासकर संजय गांधी के सामने वे बेबस और लाचार नजर आती थी। संजय गांधी सरकारी सता के इतर बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हो गए थे। इस तथ्य को प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के प्रधान सचिव रहें पीएन धर ने अपनी पुस्तक: ‘इन्दिरा गांधी, आपातकाल और भारतीय लोकतंत्र’ में भी दर्ज किया है।
प्रधानमंत्री आवास गैर संवैधानिक गतिविधियों का केन्द्र बन गया था। प्रधानमंत्री दफ्तर कमजोर हो गया था। संजय गांधी और हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल उस दौर में कांग्रेस में बढ़त हासिल कर ली थी।” ऐसे माहौल में स्वाभाविक तौर सत्ता जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होती और सरकार के निरंकुश होने का खतरा बढ़ जाता है।
सन् 1976 के मध्य में संविधान में परिवर्तन करने के लिए प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने कांग्रेस नेता देवकांत बरुआ, रजनी पटेल और सिद्धार्थ शंकर रे के सामने इस बाबत सुझाव देने और एक दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। सन् 1976 के अन्त आते-आते संजय गांधी ने मन बना लिया था कि भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह राष्ट्रपति प्रणाली लागू किया जाए और उसे प्रधानमंत्री से ज्यादा अधिकार सम्पन्न बना दिया जाए।
कुछ लोग इस राय के थे कि संजय गांधी खुद राष्ट्रपति बनाना चाहते थे़ जिस समय संविधान बदलने की बात चल रही थी उसी समय एक बातचीत का हवाला देते हुए बताया गया है कि- संजय गांधी के चाटुकार मण्डली में शामिल बंसीलाल ने इन्दिरा गांधी के चचेरे भाई बीके नेहरू से कहा कि-“
चुनाव जैसी बेवकूफी से छुटकारा पाइए। बस हमारी बहन इन्दिरा जी को जीवन भर के लिए राष्ट्रपति बनवा दीजिए। इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। ” ये वहीं बंसीलाल थे, जो सन् 1975 से सन् 1977तक देश के रक्षा मंत्री भी रहें।
नीरजा चौधरी बताती हैं कि संविधान में परिवर्तन के लिए जो दस्तावेज इन्दिरा गांधी को सौंपा गया था, उसे स्वयं देवकांत बरुआ ने ही ‘लीक’ किया। संजय गांधी और उनकी मण्डली के दबाव में तब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के विधानसभाओं से संविधान में व्यापक बदलाव के लिए प्रस्ताव भी पारित करवाया गया। संविधान में परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य था, चुनाव स्थगित करना, आपातकाल को जारी रखना और इस प्रकार श्रीमती इन्दिरा गांधी की सत्ता को हर लिहाज से अक्षुण्ण बनाए रखना। हालांकि पी एन धर लिखते है कि इन्दिरा गांधी विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित करवाने को लेकर चिन्तित थी।
इंदिरा गांधी की सियासत डगमगाने लगी
इन्दिरा गांधी की सत्ता के विरुद्ध संकट तब से ही मंडराने लगे थे। इन्दिरा गांधी की अपनी छवि इसके पहले एक निर्णायक और बेहद दुस्साहसी लौह महिला की थी। अब वे संजय गांधी के सामने लाचार और बेबस मां नज़र आने लगी थी। राजनीतिक नेतृत्व की असली परीक्षा ऐसे मौके पर ही होती है। मोह ज्ञान को नष्ट कर देता है। यह शिक्षा श्रीमद भागवत् गीता से भी प्राप्त होती है। पर ऐसा लगता है कि श्रीमती गांधी पुत्र मोह से उबर नहीं पा रही थी। उधर संजय गांधी की चाटुकार मण्डली उस मोह को लगातार प्रज्वलित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे।
12 जून सन् 1975 का दिन शायद इन्दिरा गांधी के तब तक के राजनीतिक जीवन में सबसे मुश्किल दिन रहा होगा। इस दिन तीन घटनाएं एक साथ घटित हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के अनुसार इन्दिरा गांधी को छह साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया। इन्दिरा गांधी गांधी के बेहद करीबी रहें डीपी धर की मृत्यु का दुःखद समाचार मिला। तब वे मास्को में भारत के राजदूत थे। उसी दिन रात तक गुजरात विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस की हार हुई। अपने 258 पेज के इस फैसले को लिखवाने में जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने बेहद गोपनीयता बरती थी। यहां तक कि 11 जून को फैसला लिखवाने के बाद वे अपने टाइपिस्ट नेगीराम को कहीं गायब हो जाने के लिए कहा।
उस दौर में भी हालांकि एक हद तक राजनीति में लोकलाज और नैतिकता बची हुई थी। नेहरू के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे की की कृष्णामचारी को हरीदास मुंदड़ा काण्ड में लिप्त होने के कारण पदत्याग करना पड़ा था। कांग्रेस के सांसद फिरोज गांधी ने यह आरोप लगाया था कि ‘इंश्योरेन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ ने कलकत्ता के उघोगपति हरिदास मूंदड़ा के फर्म में एक करोड़ 1.26 करोड़ का ‘ओवरवैल्यूड’ शेयर खरीदकर मदद पहुंचाया था।
एम सी छागला आयोग ने इस आरोप को सही पाया, फलस्वरूप टी टी कृष्णामचारी को वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे तमाम आरोप मौजूदा सरकार और इसके पहले की सरकारों पर अब भी लगाया जाता है।पर अब ऐसे किसी मामले की जांच कराने और दोष सिद्ध होने पर भी इस्तीफा देने का दबाव सत्ता पक्ष की ओर से बनाने की परिपाटी खत्म हो चुकी है। अब किसी सरकार का मंत्री ‘थेथरई’ की सारी हदें पार कर, तब तक मंत्रिमंडल का सदस्य बने रहता हैं, जब तक साफ-साफ कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला नहीं सुना देता।
इन्दिरा गांधी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के आलोक में अगर इस सवाल पर विचार करें कि अगर इन्दिरा गांधी तब नैतिकता की दुहाई देकर पद त्याग देती। अपने किसी विश्वसनीय को प्रधामनंत्री बनवा देती, तो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति आंदोलन का क्या हश्र होता? ऐसी मिसाल खुद इन्दिरा गांधी ने चेन्ना रेड्डी के मामले में अथवा जब नीलम संजीव रेड्डी जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो ‘बसरूट’ के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर हाई कोर्ट में जब उनकी आलोचना हुई, तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे द्वारिका प्रसाद मिश्र जब चुनाव में अयोग्य ठहराए गए तो उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो नैतिकता की दुहाई देकर श्रीमती इन्दिरा गांधी से इस्तीफा देने की मांग कर रहें थे, उन्होंने ने ही त्रिभुवन नारायण सिंह विधानसभा का उपचुनाव हार जाने के बाद, उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने का समर्थन कर रहें थे। इस मुहिम में खुद राजनारायण भी शामिल थे।
आपातकाल के बाद 50 साल बाद
आज इस प्रसंग में यह सवाल नये सिरे उठाने की जरूरत है कि क्या लोकतंत्र में नैतिकता का दोहरा मापदंड हो सकता है?अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को इन्दिरा गांधी के खिलाफ फैसले की जानकारी थी। पुपुल जयकर (जो इन्दिरा गांधी के बेहद करीबी थी) लिखती है कि-
जयप्रकाश नारायण ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताया था कि उनके पास पक्की खबर है कि फैसला इंदिरा गांधी के विरोध में आने वाला है।”
रॉ के प्रमुख आर एन काव ने भी श्रीमती इन्दिरा गांधी को सूचित किया था कि फैसला उनके विरुद्ध आने वाला है। ऐसा नहीं था कि श्रीमती गांधी ने अपनी ओर से अपने बचाव के लिए कोई कोशिश नहीं किया। अपनी पुस्तक ‘जजमेंट’ में कुलदीप नैयर बताते है कि जस्टिस जगमोहन सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने से लेकर 50000/ रुपए की रिश्वत देने का भी लालच दिया गया।
गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के जरिये उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सूचना दी गई कि इस फैसले को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए, क्यों कि श्रीमती इन्दिरा गांधी विदेश दौरे पर जाने वाली थी। पर जस्टिस जगमोहन सिन्हा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। राजनारायण का केस प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण लड़ रहे थे। जनता पार्टी की सरकार बनने पर वे देश के कानून मंत्री बनें। पर अजीब विडंबना यह हुई कि जे पी आन्दोलन की कोख से निकले तमाम नेताओं ने जे पी को वैसे ही भूला देना ही बेहतर समझा जैसे महात्मा गांधी को आजादी के तुरन्त बाद कांग्रेस नेतृत्व ने दर किनार कर दिया। अब तक दुनिया के जनांदोलनों से यहीं सबक मिलता है कि – आन्दोलनों के बाद सत्तासीन नेतृत्व ने उन आदर्शों की बलि चढ़ा देता हैं, जिसका वादा वे आन्दोलन के दौरान करते हैं।
इस वजह से जनता का सत्ता से मोहभंग पैदा होता है और जनता ऐसी सत्ता को बेदखल करने के उपाय सोचने लगती हैं। मौका मिलते ही ऐसे सत्ताधीशों को कठोर सजा देती है। बहुत दिनों तक उन्हें सत्ता के करीब फटकने नहीं देती। कांग्रेस और गैर कांग्रेसवादी दलों के साथ अब तक तो ऐसा होता ही आया है। इस लिए सत्ता के प्रति आत्ममुग्धता और निरंकुशता से सदैव परहेज करना चाहिए । यह किसी सत्ताधारी पार्टी के लिए न्यूनतम अनिवार्य शर्त होनी चाहिए। भारतीय राजनीति का सबक तो हमें यहीं सिखाता है।